सेक्युलरिज़्म: भारतीय सिनेमा की आत्मा या सामंती मुखौटा ? - प्रोफेसर देव प्रकाश मिश्रा
Editor : Shubham awasthi | 02 September, 2025
भारतीय सिनेमा को लंबे समय से "सेक्युलरिज़्म की प्रयोगशाला" कहा जाता है। परदे पर नायक कभी मंदिर में आरती करता है, कभी मस्जिद में सजदा करता है और कभी गुरुद्वारे में मत्था टेकता है—दर्शक तालियाँ बजाकर खुश हो जाते हैं
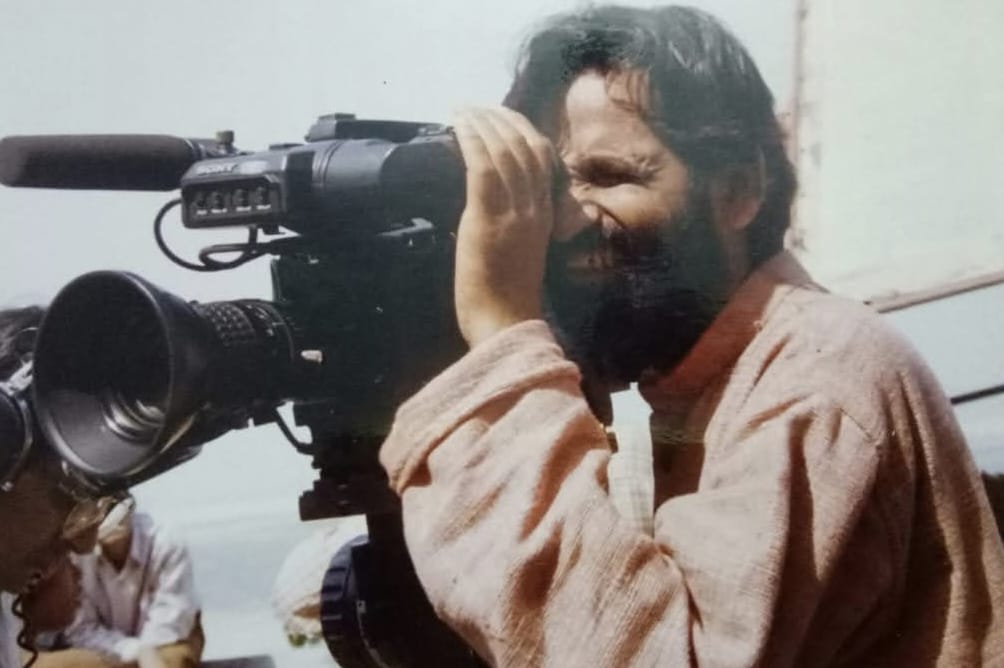
Source or Copyright Disclaimer
दशकों से यही दृश्य “गंगा-जमुनी तहज़ीब” का आईना कहकर दिखाए जाते रहे हैं।
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यही सेक्युलरिज़्म है? या यह केवल एक सामंती परंपरा का नक़ाब है—जहाँ दिखावा बहुत है, लेकिन समाज की असली विविधता और गहराई कहीं खो जाती है?
सतही धर्मनिरपेक्षता का चोला
हिंदी फिल्मों में धर्मनिरपेक्षता अक्सर सतही रही है। गानों में अल्लाह-ईश्वर का नाम साथ ले लिया, त्योहार पर नायक-नायिका ने नाच लिया—बस, यही सेक्युलरिज़्म!
लेकिन पर्दे के पीछे वही पुराना ढर्रा कायम रहा। दलित और आदिवासी तो अब भी लगभग गायब हैं।
पुरानी परंपरा से आज तक
70–80 के दशक की अमर अकबर एंथनी को “धार्मिक एकता” का प्रतीक माना गया, पर असल में यह केवल मेल-मिलाप का रंगीन तमाशा था। सामाजिक न्याय की गंभीर चर्चा कहीं नहीं थी।
आज भी तस्वीर बहुत नहीं बदली। फर्क सिर्फ़ इतना है कि अब यह तमाशा और आधुनिक पैकेजिंग में सामने आता है।
2020 के बाद की फिल्मों की तस्वीर
हाल के वर्षों में भी सेक्युलरिज़्म का असली चेहरा परदे पर कम ही दिखा।
शेरशाह (2021) और साम बहादुर (2023) जैसी देशभक्ति फिल्मों में सैनिकों का धर्म गौण रखा गया, लेकिन धार्मिक विविधता को सकारात्मक रूप में गहराई से दिखाने का साहस नहीं हुआ।
कश्मीर फाइल्स (2022) और केरला स्टोरी (2023) जैसी विवादास्पद फिल्मों ने तो धर्मनिरपेक्षता की जगह धार्मिक ध्रुवीकरण को और मज़बूत किया। ये फिल्में सेक्युलरिज़्म की प्रयोगशाला नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री बन गईं।
वहीं जय भीम (2021, तमिल) और फंड्री की परंपरा को आगे बढ़ाती कुछ मराठी और मलयालम फिल्में हाशिए पर खड़े समाज की असल कहानियाँ सामने लाईं। जय भीम ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में ला दिया।
आर्टिकल 15 की तर्ज़ पर 2020 के बाद आई भीष्मा पर्वम (मलयालम, 2022) जैसी फिल्मों ने धार्मिक और सामाजिक विविधता को जटिल लेकिन ईमानदार अंदाज़ में दिखाने की कोशिश की।
दर्शक और सिनेमा का द्वंद्व
समस्या यह है कि दर्शक अब भी त्योहार वाले गानों और मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारे वाले दृश्यों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब असली सामाजिक विविधता और संघर्ष की कहानियाँ आती हैं—तो या तो उन्हें “पैरेलल सिनेमा” का ठप्पा देकर किनारे कर दिया जाता है, या उन्हें विवादास्पद कहकर दबा दिया जाता है।
आज भारतीय सिनेमा को यह तय करना होगा कि सेक्युलरिज़्म उसके लिए मात्र धार्मिक सजावट है या सचमुच समाज की विविधता की अभिव्यक्ति।
जब तक पर्दे पर दलित, आदिवासी, मुस्लिम, उत्तर-पूर्वी समुदाय और प्रवासी मजदूरों की कहानियाँ बराबरी से नहीं आएँगी, तब तक यह सेक्युलरिज़्म अधूरा ही रहेगा।
सेक्युलरिज़्म भारतीय सिनेमा की आत्मा है—यह बात सही है। लेकिन अगर यह आत्मा सिर्फ़ चमकदार पैकेज और सामंती मानसिकता का मुखौटा बनकर रह जाए, तो यह आत्मा नहीं, महज़ नक़ाब है।
समय की मांग है कि सिनेमा इस नक़ाब को उतारे और समाज के हर चेहरे को ईमानदारी से परदे पर लाए। तभी यह कला सचमुच लोकतंत्र का आईना बन पाएगी।




