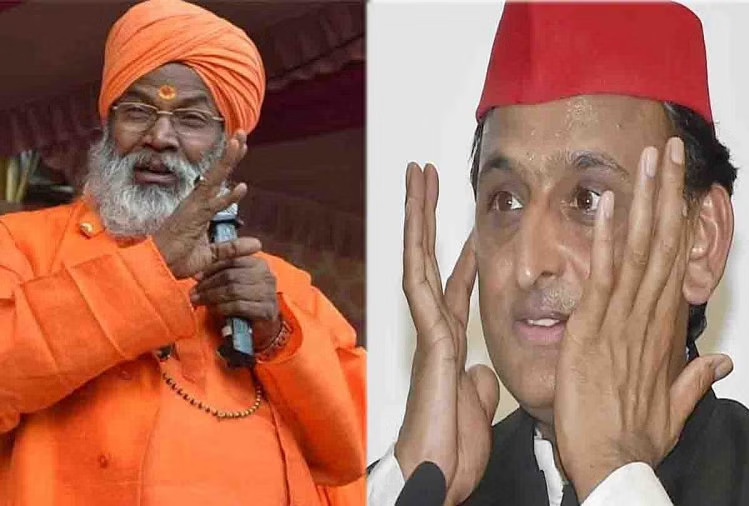लोकतंत्र की कसौटी पर नया विधेयक -प्रोफेसर देव प्रकाश मिश्र।
Editor : Shubham awasthi | 30 August, 2025
भारतीय लोकतंत्र का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही विरोधाभासों से भरा भी है। संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि सत्ता में बैठे लोग जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करेंगे, और लोकतंत्र केवल प्रक्रियाओं का नहीं बल्कि नैतिकता का भी उत्सव होगा

Source or Copyright Disclaimer
48 घंटे बनाम 30 दिन: लोकतांत्रिक असमानता
किसी भी सरकारी कर्मचारी पर यदि आपराधिक आरोप में गिरफ्तारी होती है और वह 48 घंटे से अधिक जेल में रहता है, तो केंद्रीय सेवा नियमावली (Conduct Rules & Service Rules) के तहत उसे तत्काल निलंबित कर दिया जाता है। इस कठोर प्रावधान का उद्देश्य है कि सेवा की शुचिता पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे।
इसके विपरीत, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री—जो सीधे जनता के प्रतिनिधि हैं—उन पर ऐसे नियम लागू नहीं होते। उन्हें केवल तभी अयोग्य घोषित किया जाता है जब अदालत द्वारा उन्हें दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाए। यानी, जब तक अदालत दोषसिद्धि नहीं करती, तब तक वे सत्ता में बने रह सकते हैं, चाहे वे जेल की सलाखों के पीछे ही क्यों न हों।
इस दोहरे मानक ने ही राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है। जबकि आम सरकारी कर्मचारी पर सख्ती है, जनता के प्रतिनिधि को छूट मिली हुई है।
नया विधेयक: संविधान का 130वाँ संशोधन
इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में “संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025” पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को रखते हुए तर्क दिया कि लोकतंत्र में जवाबदेही को और कठोर बनाने की आवश्यकता है।
यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार होते हैं, जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, और वे लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो वे स्वतः पद से अयोग्य हो जाएंगे।
दोषसिद्धि का इंतज़ार नहीं होगा; गिरफ्तारी और निरंतर हिरासत ही पदच्युति का आधार होगी।
यदि आरोपी को ज़मानत मिल जाए, तो वह दोबारा पद ग्रहण कर सकता है।
नैतिकता की ओर एक कदम?
पहली नज़र में यह प्रावधान स्वागत योग्य लगता है। इससे राजनीतिक दलों को अपने टिकट वितरण और नेतृत्व चयन में अधिक सावधानी बरतनी होगी। जनता के सामने यह संदेश जाएगा कि सत्ता की बागडोर अब उन हाथों में नहीं होगी जो गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे हैं।
1. दिल्ली – अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद भी उन्होंने जेल से ही सरकार चलाने की कोशिश की। यह लोकतंत्र की गंभीर विडंबना थी।
2. झारखंड – हेमंत सोरेन भी कानूनी शिकंजे में फँसने के बावजूद सत्ता में बने रहे और सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश की।
ऐसे मामलों ने जनता का भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कमजोर किया है। नया विधेयक इस स्थिति को बदलने का प्रयास करता है।
विपक्ष की आशंका
लेकिन लोकतंत्र केवल आदर्शों से नहीं चलता, उसकी सफलता निष्पक्ष प्रक्रियाओं पर भी निर्भर करती है। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक लोकतंत्र की आत्मा के लिए खतरनाक है।
गिरफ्तारी का अर्थ दोषसिद्धि नहीं होता। भारतीय न्याय व्यवस्था में मुकदमों का लंबा सिलसिला और एजेंसियों पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में, यदि महज़ गिरफ्तारी और 30 दिन जेल को ही अयोग्यता का आधार बना दिया जाए, तो सत्ता में बैठी सरकार विरोधियों को कुचलने के लिए इसे हथियार बना सकती है।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार किया गया था और वे महीनों जेल में रहे, लेकिन बाद में जमानत पर बाहर आ गए। यदि नया कानून तब लागू होता, तो उनकी राजनीतिक भूमिका स्वतः समाप्त हो जाती, भले ही अदालत ने उन्हें दोषी सिद्ध न किया हो।
लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दोषसिद्ध हुए, लेकिन उससे पहले वर्षों तक केवल मुकदमेबाज़ी होती रही। गिरफ्तारी की अवधि को अयोग्यता का आधार बनाने पर सवाल उठता कि कहीं यह केवल राजनीतिक विरोध को दबाने का जरिया तो नहीं बन जाएगा।
लोकतांत्रिक विरोधाभास
लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है। और जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी कर्मचारियों से भी ऊँचे नैतिक मानकों पर खरे उतरें। लेकिन व्यवहारिक राजनीति ने इसे उल्टा कर दिया—सरकारी कर्मचारी पर सख्ती, और जनप्रतिनिधि पर ढील। यही विरोधाभास आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है।
राजनीति और चुनावी मायने
इस विधेयक का समय और संदर्भ भी महत्त्वपूर्ण है। 2025 के बाद देश में बड़े राज्यों के चुनाव और फिर आम चुनाव आने वाले हैं। भाजपा इस बिल को अपने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे के रूप में प्रचारित करेगी।
यदि विपक्ष इसका समर्थन करता है, तो भाजपा कहेगी—“देखो, हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं।”
यदि विपक्ष इसका विरोध करता है, तो भाजपा का आरोप होगा—“ये लोग भ्रष्टाचारियों के हिमायती हैं।”
यानी, राजनीतिक दृष्टि से यह भाजपा के लिए दोनों तरफ़ से लाभकारी मुद्दा है।
JPC और संसदीय प्रक्रिया
संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। इस प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट भी आएगी। संभावना यही है कि JPC कुछ औपचारिक सुझाव देगी, लेकिन बहुमत के बल पर सरकार इसे पास करा लेगी।
जनता का नजरिया
सबसे बड़ा प्रश्न जनता का है। क्या यह कानून सचमुच राजनीति को स्वच्छ बनाएगा, या फिर यह केवल सत्ता की राजनीति का नया औज़ार बनेगा?
यदि इसे निष्पक्षता और सख्ती से लागू किया गया, तो यह राजनीति में अपराधियों की प्रविष्टि रोकने की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। इससे जनता का लोकतंत्र पर विश्वास मजबूत होगा।
लेकिन यदि यह सिर्फ एजेंसियों के दुरुपयोग का जरिया बना, तो जनता इसे तानाशाही की ओर कदम मानेगी। लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर यह और बड़ा धब्बा होगा।
“30 दिन बनाम 48 घंटे” का अंतर केवल समय की गणना नहीं है—यह लोकतंत्र की आत्मा का प्रश्न है। यदि यह विधेयक सही मायनों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, तो यह भारतीय राजनीति को नई गरिमा देगा। लेकिन यदि यह सत्ता का नया हथियार बन गया, तो लोकतंत्र पर से जनता का भरोसा और भी गहरा आघात झेलेगा।
लोकतंत्र का मर्म यही कहता है कि जनप्रतिनिधि जनता से अधिक जवाबदेह हों। यदि इस जवाबदेही की आड़ में लोकतंत्र की स्वतंत्रता कुचल दी गई, तो यही विधेयक भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना बन जाएगा।